कक्षा 12 समष्टि अर्थशास्त्र – Unit 5: सरकारी बजट (NCERT प्रश्न-उत्तर हिंदी में)
Unit – 5: सरकारी बजट | School Economics
प्र.1 बजट से आप क्या समझते हैं।
उत्तर: बजट एक वित्तीय वर्ष (भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक) में सरकार की अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण होता है।
बजट एक विस्तृत आर्थिक विवरण है जिसमें सरकार की एक वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का ब्यौरा होता है।
प्र.2 सरकारी बजट की परिभाषा दीजिए। या बजट की परिभाषा दीजिए।
उत्तर: रेने स्टोर्न के अनुसार: "बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक आय व सार्वजनिक व्यय की एक स्वीकृति योजना होती है।"
प्र.3 संतुलित बजट की परिभाषा दीजिए।
उत्तर: संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं।
संतुलित बजट = सरकार की आय = सरकार का व्यय
संतुलित बजट का आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके कारण न तो संकुचनकारी शक्तियां और न ही विस्तारवादी शक्तियां काम कर पाती हैं।
प्र.4 घाटे की बजट से क्या आशय है?
उत्तर: घाटे का बजट - वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से कम होती है।
घाटे का बजट = सरकार की अनुमानित आय < सरकार का अनुमानित व्यय
घाटे का बजट का तात्पर्य यह है कि सरकार जितनी मात्रा में मुद्रा अर्थव्यवस्था में खपा सकती है। उसे अधिक मात्रा में मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रवाहित कर दी जाती है। फलत: अर्थव्यवस्था में विस्तारवादी शक्तियां बलवती हो उठती हैं।
प्र.5 बचत के बजट की परिभाषा दें। या अधिक्य या अतिरेक का बजट
उत्तर: बचत या अधिक्य या अतिरेक का बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से अधिक होता है।
बचत का बजट = सरकार की अनुमानित आय > सरकार का अनुमानित व्यय
प्र.6 भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है?
उत्तर: भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। जिसमें भारत के बजट का आय व्यय का लेखा जोखा तैयार किया जाता है।
प्र.7 सरकारी बजट में राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं?
उत्तर: राजस्व या आगम प्राप्तियों में सरकार को कर राजस्व और गैर कर राजस्व मदों से प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जाता है।
अन्य शब्दों में राजस्व प्राप्तियां को दो भागों में विभाजित किया जाता है: कर राजस्व तथा गैर कर राजस्व।
प्र.8 कर की परिभाषा दीजिए।
उत्तर: डाल्टन के अनुसार: "कर लोकसत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, जिसका कर के रूप में दी जाने वाली राशि के बदले उतनी ही मात्रा में लाभ प्राप्त करने से कोई संबंध नहीं और न ही यह किसी गैर कानूनी कार्य का जुर्माना ही है।"
प्र.9 प्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए। दो उदाहरण दीजिए।
उत्तर: प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही उसका भार उठाता है, इस कर को टाला नहीं जा सकता है न ही इसका भार आंशिक या पूर्ण रूप में किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जा सकता है।
दूसरे शब्दों में जब किसी कर का कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। तब यह कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है।
प्रत्यक्ष कर का उदाहरण: आयकर, निगम कर, संपत्ति कर है।
प्र.10 अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा दीजिए। अप्रत्यक्ष कर के दो उदाहरण बताइए।
उत्तर: अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर - जो कर किसी एक व्यक्ति पर लगाए जाए परंतु उनका भुगतान पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दूसरे व्यक्ति करें, वे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करने का दायित्व तथा कर का मौद्रिक भार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है।
उदाहरण के लिए: उत्पाद कर, सीमा शुल्क, अबकारी कर, बिक्री कर, वस्तु एवं सेवा कर।
प्र.11 अनुपातिक कर की परिभाषा दीजिए।
उत्तर: अनुपातिक कर वह कर है जिसमें सभी आय स्तरों पर एक ही दर से कर लगाया जाता है। अर्थात चाहे आय घटे या बढ़े परंतु कर की दर एक समान रहती है। इस प्रकार अनुपातिक कर की दर निर्धन व्यक्तियों एवं धनी व्यक्तियों के लिए एक समान होती है।
प्र.12 प्रगतिशील कर की परिभाषा दीजिए।
उत्तर: प्रगतिशील कर वह कर है जिसकी दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। प्रगतिशील कर में कम आय स्तर पर कम दर से तथा अधिक आय स्तर पर अधिक दर से कर आरोपित किया जाता है।
प्र.13 प्रतिगामी कर क्या है?
उत्तर: प्रतिगामी कर उस कर को कहते हैं जिसका भार अमीरों की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़ता है, अर्थात जैसे-जैसे कर योग्य आय बढ़ती जाती है कर की दर घटती जाती है।
प्र.14 गैर कर राजस्व के दो स्रोत लिखिए। या उदाहरण
उत्तर: गैर कर आगम या राजस्व का आशय उस प्राप्ति से है जो सरकार को कर को छोड़कर अन्य साधनों से होती है उदाहरण के लिए ब्याज, लाभ तथा लाभांश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना तथा दंड, उपहार एवं अनुदान, जब्ती आदि।
प्र.15 पूंजीगत प्राप्तियां सरकारी बजट में क्या होती हैं?
उत्तर: पूंजीगत प्राप्तियों अंतर्गत आय के उन समस्त स्रोतों को रखा जाता है जिसका हमें बदले में भुगतान करना अवश्य होता है, लेकिन महत्वपूर्ण यहां है कि भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में ना होकर आगामी किसी वित्तीय वर्ष में किए जाते हैं। इसे पूंजी खाता नाम से जानते हैं। इस प्रकार राजस्व प्राप्तियों की प्रकृति जहां अल्पकालीन किस्म की होती है वहीं पूंजीगत प्राप्तियों की प्रकृति दीर्घकालीन होती है।
प्र.16 उधारी को पूंजीगत प्राप्तियों में क्यों शामिल किया जाता है?
उत्तर: पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आय के उन समस्त स्रोतों को रखा जाता है जिनका हमें बदले में भुगतान करना अवश्य होता है लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में ना होकर आगामी किसी वित्तीय वर्ष में किए जाते हैं।
अतः उधारी का भुगतान भी भविष्य में करना पड़ता है इसलिए इसे पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किया जाता है।
प्र.17 राजस्व व्यय क्या है?
उत्तर: राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही देयता में कमी होती है।
उदाहरण के लिए सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति आदि साथ ही साथ ऋणों के भुगतान पर किए गए व्यय।
प्र.18 राजस्व प्राप्तियों की परिभाषा दीजिए।
उत्तर: वे प्राप्तियां जो न तो देयताओं का निर्माण करती हैं और न ही परिसंपत्तियों को कम करती हैं वे राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं उदाहरण के लिए कर, सार्वजनिक उद्योगों के शेयर का विक्रय आदि।
प्र.19 राजकोषीय घाटे की परिभाषा दीजिए।
उत्तर: राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के व्ययों तथा राजस्व और उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से है।
राजकोषीय घाटा कुल व्यय (राजस्व + पूंजीगत) की उधार छोड़कर कुल प्राप्तियों (राजस्व + उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों) पर अधिकता है।
प्र.20 पूरक बजट किसे कहते हैं?
उत्तर: पूरक बजट - पूरक बजट वह बजट है जो किसी देश की सरकार के द्वारा युद्ध, भूकंप, बाढ़ जैसे अल्पकालीन परिस्थितियों में संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस बजट के लिए कोई निश्चित समयावधि नहीं होती।
प्र.21 प्राथमिक घाटा क्या होता है?
उत्तर: प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे तथा भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर है।
प्राथमिक घाटा या सकल प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
प्र.22 योजनागत व्यय क्या है?
उत्तर: योजनागत व्यय उस व्यय को कहते हैं जो सरकार द्वारा देश के योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम पर किया जाता है उदाहरण के लिए सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय योजनागत व्यय है।
प्र.23 गैर योजनागत व्यय क्या है?
उत्तर: गैर योजना व्यय से अभिप्राय उस व्यय से है जिसका योजनाओं में कोई प्रावधान नहीं किया जाता।
प्रत्येक योजना की समाप्ति पर उस योजना में शुरू किए गए कार्यक्रम योजना की अवधि से बाहर आ जाते हैं। कार्यक्रमों के संपादन पर होने वाले चालू व्ययों को गैर योजना व्यय कहते हैं। इस तरह के व्यय की व्यवस्था प्रत्येक बजट में की जाती है।
प्र.24 विकासात्मक व्यय क्या है? दो उदाहरण दीजिए।
उत्तर: ऐसा व्यय जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास से सीधा संबंध रखता है विकासात्मक व्यय कहलाता है। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक कल्याण, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर किया गया व्यय विकासात्मक कहलाता है।
प्र.25 अंतरिम बजट किसे कहते हैं?
उत्तर: अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। इसे लेखानुदान मांग और मिनी बजट भी कहते हैं। वोट ऑन अकाउंट के द्वारा सीमित अवधि के लिए केंद्र सरकार के आवश्यक खर्चों को स्वीकृति दी जाती है। जिस वर्ष लोकसभा का चुनाव होता है उस वर्ष सरकार अंतरिम बजट प्रस्तुत करती है। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट प्रस्तुत करती है।
प्र.26 राजकोषीय घाटे का क्या महत्व है?
उत्तर: राजकोषीय घाटे का महत्व - राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था को दिशा निर्देश प्रदान करने के रूप में एक उपयोगी उपकरण हो सकता है क्योंकि:
- इसकी सहायता से अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय की राशि में वृद्धि संभव हो पाती है।
- सरकार अपने व्ययों की आपूर्ति के लिए अधिक वित्तीय संसाधन जुटा पाती है।
प्र.27 कर क्या है इसकी विशेषताएं लिखिए?
उत्तर: कर का अर्थ - कर प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जो सरकार कर तथा शुल्क लगाकर अर्जित करती हैं।
कर की विशेषताएं:
- कर एक अनिवार्य अंशदान है।
- कर से होने वाली आय का उपयोग सामान्य हित के लिए किया जाता है।
- सरकार करदाता को कर के बदले में कोई विशेष लाभ नहीं प्रदान करती।
- कर वस्तुओं तथा संपत्ति पर लगाया जाता है परंतु इसका भुगतान व्यक्ति ही करते हैं। यह उनका निजी कर्तव्य माना जाता है।
- करदाता को त्याग करना पड़ता है, किंतु यह प्रतिफल रहित त्याग है। कर सेवा का लागत मूल्य नहीं है।
- करारोपण वैधानिक सत्ता पर आधारित और निर्धारित होता है।
प्र.28 प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए।
उत्तर:
| प्रत्यक्ष कर | अप्रत्यक्ष कर |
|---|---|
| वह कर जो आय एवं संपत्ति पर लगाए जाते हैं प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। | वे कर जो वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाते हैं अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। |
| इन करों का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिन पर यह लगाया जाता है। | अप्रत्यक्ष करों का भार दूसरों पर डाला जा सकता है। |
| कर का भार धनी पर अधिक एवं निर्धनों पर कम पड़ता है। यह कर प्रगतिशील कहलाते हैं। आय के बढ़ने से इनकी दर भी बढ़ जाती है। | अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव निर्धनों एवं धनी पर एक जैसा पड़ता है। यह कर अनुपाती होते हैं। |
| आयकर, मृत्यु कर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यवसाय कर, प्रत्यक्ष करों में शामिल होते हैं। | बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद कर, टोल कर, सेवा कर, मूल्य संवर्धित कर, वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर हैं। |
प्र.29 सरकारी बजट का क्या महत्व है? समझाइए।
उत्तर: बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं से जाना जा सकता है:
- आर्थिक नियंत्रण: बजट सरकार के विभिन्न विभागों के आय-व्यय को नियंत्रित करता है।
- आर्थिक स्थिरता: आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार मंदी में घाटे का बजट एवं तेजी में अधिक्य का बजट बनाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करती है।
- अधिकारियों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण: बजट द्वारा सभी अधिकारियों के कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित कर दी जाती है ताकि वे उत्तरदायित्व का उचित निर्वहन कर जनता का आर्थिक कल्याण कर सकें।
- सार्वजनिक उपक्रमों से लाभ: बजट में सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ हानि का ब्यौरा भी होता है जिससे जानकारी मिलती है कि कितने उद्योग लाभ और कितने हानि में चल रहे हैं।
- विदेशी विनिमय: बजट में विदेशी मुद्रा भंडार में ऋण पर ब्याज, विदेशी निवेश एवं विनिमय दर के साथ विनिमय दशाओं का भी उल्लेख होता है जिससे इसके संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है।
- कर और गैर कर साधनों में समन्वय: सरकार बजट के माध्यम से कर आय और गैर कर आय साधनों में समन्वय स्थापित करती है।
- शासकीय नीतियों का ज्ञान: बजट से सरकारी नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है। सरकार की राजकोषीय, मौद्रिक, औद्योगिक एवं व्यापारिक नीति का ज्ञान होता है।
प्र.30 राजस्व घाटे तथा वित्तीय घाटे में अंतर समझाइए।
उत्तर:
| राजस्व घाटा | वित्तीय घाटा |
|---|---|
| जब राजस्व व्यय राजस्व आय से अधिक हो तो यह अधिक्य की स्थिति राजस्व घाटा कहलाती है। | जब कुल व्यय प्राप्तियों की राशि से अधिक हो तो यह अधिक्य की स्थिति वित्तीय घाटा कहलाती है। ध्यान रहे इसमें उधारी की राशि शामिल नहीं रहती। |
| राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व आय | वित्तीय घाटा यह दर्शाता है कि सरकार को कितनी राशि उधारी के रूप में लेने से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी। |
प्र.31 प्राथमिक घाटे तथा वित्तीय घाटे में अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
| प्राथमिक घाटा | वित्तीय घाटा |
|---|---|
| यह वित्तीय घाटे तथा ब्याज के भुगतान का अंतर होता है। | यह कुल व्यय का कुल प्राप्तियों पर अधिक्य है। कुल प्राप्तियों में उधारी शामिल नहीं होती। |
| यह इस बात का संकेत है कि सरकार को ब्याज की राशि छोड़कर कितनी राशि उधार लेना आवश्यक है। | यह इस बात का संकेत है कि ब्याज सहित सरकार की कितनी राशि उधार लेने से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। |
| प्राथमिक घाटा = वित्तीय घाटा - ब्याज का भुगतान | वित्तीय घाटा = कुल व्यय - कुल प्राप्तियां (उधारी की रकम छोड़कर) |
प्र.32 राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर समझाइए।
उत्तर:
| राजस्व प्राप्तियां | पूंजीगत प्राप्तियां |
|---|---|
| राजस्व प्राप्तियां सरकार की न तो देयता उत्पन्न करती हैं और न ही परिसंपत्तियों में वृद्धि करती हैं। | पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की देयता उत्पन्न करती हैं एवं परिसंपत्तियों में कमी करती हैं। |
| कर, शुल्क, चालान, जुर्माने से प्राप्त आय राजस्व प्राप्तियों में शामिल होती है। | ऋण प्राप्त करना देयताओं को बढ़ाता है एवं विनिवेश सरकारी परिसंपत्तियों में कमी करता है। |
| यह आवृत्ति की स्वभाव की होती है, बार-बार प्राप्त होती है। इनकी पुनरावृत्ति अधिक होती है। | यह अनावृत्ति स्वभाव की होती है अर्थात इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। |
प्र.33 राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में क्या भेद है? समझाइए।
उत्तर:
| राजस्व व्यय | पूंजीगत व्यय |
|---|---|
| राजस्व व्ययों का स्वभाव आवृत्ति होता है, यह बार-बार किए जाते हैं। | पूंजीगत मदों का स्वभाव अनावृत्ति होता है, यह बार-बार नहीं किए जाते। |
| इसमें प्रतिरक्षा, नागरिक प्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं शिक्षा की मदें शामिल होती हैं। | पूंजीगत व्यय में भवन एवं बांध निर्माण, मशीनों की स्थापना आदि आते हैं। |
| यह व्यय गैर विकासात्मक कहलाते हैं। | यह व्यय विकासात्मक कहलाते हैं। |
| यह व्यय अल्पकालीन होते हैं। | यह व्यय दीर्घकालीन होते हैं। |
प्र.34 बजट की विशेषताएं लिखिए। या नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट की विशेषताएं लिखिए।
उत्तर: नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट की विशेषताएं:
- नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट राष्ट्रीय नियोजन के वृहद उद्देश्य पर आधारित होता है।
- नियोजन के प्रारंभिक काल में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर प्रायः घाटे का बजट बनाया जाता है तथा बाद में बजट को धीरे-धीरे संतुलित करने का प्रयास किया जाता है।
- नियोजित अर्थव्यवस्था में बजट का निर्माण इस तरह किया जाता है कि कर का प्रभाव अधिकाधिक न्यायपूर्ण रहे। इसके लिए प्रगतिशील कर की नीति अपनाई जाती है।
- देश की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में बजट की भूमिका सकारात्मक होती है।
प्र.35 प्रत्यक्ष कर के लाभों का वर्णन कीजिए।
उत्तर: प्रत्यक्ष करों के गुण या लाभ निम्नलिखित हैं:
- न्यायपूर्ण: प्रत्यक्ष कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि यह व्यक्तिगत आय क्षमताओं के आधार पर लगाए जाते हैं।
- प्रगतिशील: करदाता की आय अधिक होने पर कर की दर भी बढ़ती जाती है। प्रगतिशील कर आय की असमानता को कम करते हैं।
- निश्चित: इन करों में अनिश्चितता का गुण पाया जाता है क्योंकि करदाता को कब कितना कहां कैसे कर जमा करना है।
- लोचशील: ये कर लोचपूर्ण होते हैं क्योंकि सरकार संकट के समय की आवश्यकता पड़ने पर इनकी दरों में वृद्धि या कमी कर सकती है।
- उत्पादकता: प्रत्यक्ष कर उत्पादक भी होते हैं।
- मुद्रा प्रसार के प्रभाव को रोकने में सहायक: प्रत्यक्ष करों के माध्यम से मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण लगाया जा सकता है।
- कर भार दूसरे पर नहीं: प्रत्यक्ष कर में कर भार करापात एवं कराघात एक ही व्यक्ति पर होता है।
प्र.36 अप्रत्यक्ष कर के क्या लाभ हैं? समझाइए।
उत्तर: अप्रत्यक्ष या परोक्ष करों के गुण या लाभ निम्नलिखित हैं:
- सुविधाजनक: अप्रत्यक्ष कर करदाता को कर चुकाने में सुविधाजनक होते हैं।
- न्यायोचित: यह कर प्रायः वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाए जाते हैं अतः उपभोग प्रवृत्ति के अनुसार यह न्यायोचित होते हैं।
- कर वंचन कठिन: अप्रत्यक्ष करों में कर चोरी की कम संभावना होती है।
- लोचदार: अप्रत्यक्ष कर बहुत लोचदार होते हैं क्योंकि अनिवार्य वस्तुओं पर कर की दर में थोड़ी सी वृद्धि करने पर इनमें बहुत अधिक आय प्राप्त होती है।
- सामाजिक लाभ: हानिकारक वस्तुओं जैसे शराब, भांग, गांजा, चरस आदि पर ऊंची दर से कर लगाकर इनको महंगा किया जा सकता है।
- लोकप्रिय: यह कर बहुत ही लोकप्रिय होते हैं क्योंकि इनके भुगतान करने में करदाता को बहुत अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता।
प्र.37 प्रत्यक्ष कर के दोषों को समझाइए।
उत्तर: प्रत्यक्ष करों के दोष एवं हानियां या सीमाएं निम्नलिखित हैं:
- असुविधाजनक: प्रत्यक्ष कर असुविधाजनक होते हैं उन्हें चुकाने में करदाता को कष्ट होता है।
- कर चोरी: प्रत्यक्ष करों में कर चोरी की संभावना बहुत अधिक होती है।
- खर्चीले: प्रत्यक्ष करों को वसूल करने में सरकार को बहुत अधिक खर्च उठाना पड़ता है।
- समानता: इन करों का भार पूछे लोगों पर पड़ता है।
- अनुत्पादक: सरकार को इनसे बहुत कम आय प्राप्त होती है।
- मानसिक पीड़ा: कर को चुकाने वाले व्यक्ति को मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है।
प्र.38 अप्रत्यक्ष कर के दोषों को समझाइए।
उत्तर: अप्रत्यक्ष या परोक्ष करों के दोष हानियां या सीमाएं निम्नलिखित हैं:
- न्याय संगत नहीं: अप्रत्यक्ष कर न्याय संगत नहीं होते हैं। यह वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाते हैं जिससे निर्धन और धनी वर्ग समान कर देते हैं।
- अनिश्चितता: इन करों से प्राप्त होने वाली आय अनिश्चित होती है।
- खर्चीले: इन करों को छोटी-छोटी मात्रा में वसूली करने से इनमें खर्च बहुत अधिक आता है।
- बेलोच: यह कर बेलोच होते हैं क्योंकि सरकार के द्वारा विलासिता की वस्तुओं पर कर लगाने से लोग उन्हें खरीदना कम कर देते हैं।
- कर चोरी को प्रोत्साहन: अप्रत्यक्ष कर में कर चोरी की संभावना बनी रहती है।
- नागरिक चेतना का अभाव: अप्रत्यक्ष करों में नागरिक चेतना का भाव नहीं रहता है।
प्र.39 गैर कर राजस्व के स्रोत का वर्णन कीजिए।
उत्तर: गैर कर आगम या राजस्व के साधन निम्नलिखित हैं:
- ब्याज: केंद्र सरकार को ऋण पर ब्याज प्राप्त होता है - राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों पर, केंद्र शासित क्षेत्रों को दिए गए ऋणों पर, निजी उपक्रम और सामान्य जनता को दिए गए ऋणों पर।
- लाभ तथा लाभांश: केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभ एवं लाभांश प्राप्त करती है।
- शुल्क: केंद्र सरकार विभिन्न सेवाओं जैसे न्यायालय, पंजीयन, आयात आदि के शुल्क प्राप्त करती है।
- लाइसेंस शुल्क: विभिन्न प्रकार के व्यापारी लाइसेंसों एवं परमिट पर शुल्क प्राप्त करती है।
- जुर्माना एवं दंड: कानून एवं व्यवस्था का उल्लंघन करने पर जुर्माना दंड से राजस्व प्राप्त करती है।
- उपहार एवं अनुदान: विभिन्न प्रकार के विदेशी सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, व्यक्तियों, कंपनियों आदि से उपहार एवं अनुदान प्राप्त करती है।
- जब्ती: न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के परिपालन में जब्ती से राजस्व प्राप्त करना।
प्र.40 पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत का उल्लेख कीजिए।
उत्तर: पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत निम्नलिखित हैं:
- ऋणों की वसूली: राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को जो ऋण दिए जाते हैं उनका भुगतान जब केंद्र सरकार को प्राप्त होता है तो वह पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है।
- उधारी तथा अन्य दायित्व: विभिन्न साधनों से केंद्र सरकार जो उधार लेती है जिसमें ऋण बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी सरकारों, अन्य संस्थाओं से ऋण की उधारी पूंजीगत प्राप्तियों की श्रेणी में आती है।
- विनिवेश: सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में अपने अंशों का एक भाग बेच देती है तो ऐसी प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है।
- लघु बचतें: डाकघर जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र आदि के रूप में लघु बचतों को सरकार द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें भी पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किया जाता है।
प्र.41 घाटे की बजट आप क्या समझते हैं? इसके अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए।
उत्तर: घाटे की बजट का अर्थ: घाटे के बजट से तात्पर्य ऐसी बजट व्यवस्था से है जिसमें आय की तुलना में व्यय को अधिक बताया जाता है।
- घाटे की वित्त व्यवस्था से मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है।
- घाटे के बजट से निजी निवेश में वृद्धि होती है।
- घाटे के बजट से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है।
- घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग से अर्थव्यवस्था के अनियंत्रित होने की संभावना रहती है।
- घाटे के बजट का आय के वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जिसके कारण कीमतों में वृद्धि होती है।
प्र.42 बजट के विभिन्न प्रकारों को समझाइए।
उत्तर: बजट के निम्नलिखित प्रकार हैं:
- संतुलित बजट: यदि बजट में आय और व्यय राशि समान हो तो उसे संतुलित बजट कहते हैं। यह बजट की एक आदर्श व्यवस्था है।
- असंतुलित बजट: असंतुलित बजट से आशय ऐसे बजट से है जिसमें सरकार की आय व्यय में समानता नहीं होती। असंतुलित बजट दो प्रकार का है:
- A. घाटे का बजट: घाटे के बजट में आय की तुलना में व्यय अधिक किया जाता है। उसे घाटे का बजट कहते हैं। वर्तमान में घाटे के बजट का अधिक प्रचलन है।
- B. आधिक्य का बजट: आधिक्य का बजट घाटे के बजट के विपरीत होता है। आधिक्य के बजट में आय की तुलना में व्यय कम किया जाता है।
- सामान्य बजट: जिस बजट का निर्माण सामान्य परिस्थितियों में आर्थिक आधार पर किया जाता है उसे सामान्य बजट कहते हैं।
- पूंजीगत बजट: पूंजीगत बजट के अंतर्गत केवल पूंजीगत मदों को सम्मिलित किया जाता है। इस बजट को सामान्य बजट से अलग रखा जाता है तथा व्यय को सार्वजनिक ऋणों से पूरा किया जाता है।
- आंतरिक बजट: जब सरकार किसी विशेष परिस्थितिवश पूरे वर्ष हेतू आय व्यय का अनुमान तैयार करने में असमर्थ रहती है तो वर्ष के कुछ महीनों के लिए आवश्यक आर्थिक गतिविधियों चलाने के लिए आय व्यय के प्रावधान किए जाते हैं इसे ही आंतरिक बजट कहते हैं।
प्र.43 बजट का अर्थ बताते हुए उसके उद्देश्यों को समझाइए।
उत्तर: बजट का अर्थ: बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक आय एवं सार्वजनिक व्यय की एकीकृत योजना बनाई जाती है।
बजट के उद्देश्य:
- आर्थिक विकास को प्रोत्साहन: बजट का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति को प्रोत्साहन देना होता है। बजट देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। अनिश्चितता से देश की रक्षा जा सके।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास: सरकार बजट के माध्यम से संतुलित क्षेत्रीय विकास बढ़ावा देने हेतु पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है।
- आय का वितरण: अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता में कमी करने में बजट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थव्यवस्था में पाई जाने वाली असमानता को कम करने के लिए बजट द्वारा कई उपाय किए जा सकते हैं।
- आर्थिक स्थिरता: अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते रहते हैं, जिसे नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्राप्त करना भी बजट का मुख्य उद्देश्य होता है।
- रोजगार का सृजन: रोजगार का सृजन करना ही सरकार के बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है जिसके लिए सरकार रोजगार से संबंधित योजनाओं का निर्माण करती है।
प्र.44 घाटे में कटौती के विषय में विचार विमर्श कीजिए।
उत्तर: राजकोषीय घाटे में कटौती के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
- सार्वजनिक व्ययों में कमी करके: सरकार अपने सार्वजनिक व्यय में कमी करके घाटे को कम कर सकती है।
- करों में वृद्धि करके: सरकार अपने घाटे को कम करने के लिए करों में वृद्धि करके उसे पूरा कर सकती है।
- विनिवेश करके: सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश करके सरकार बड़ी मात्रा में पूंजी प्राप्त कर सकती है एवं अपने घाटे को भी इससे कम कर सकती है।
- नये कर लगाकर: सरकार कुछ नए कर लगाकर भी अपने घाटे में कटौती कर सकती है।
प्र.45 बजट द्वारा आय की असमानताओं को कैसे दूर किया जा सकता है? या आय की असमानता को दूर करने में सरकारी बजट की क्या भूमिका है? समझाइए।
उत्तर: बजट द्वारा प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाकर, सब्सिडी देकर, और सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से आय की असमानताओं को दूर किया जा सकता है।
प्र.46 सरकारी बजट से आर्थिक स्थिरता कैसे प्राप्त की जा सकती है? संक्षेप में समझाइए।
उत्तर: सरकारी बजट से आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए मंदी में घाटे का बजट और तेजी में अधिक्य का बजट बनाया जाता है।
प्र.47 पूंजीगत बजट की परिभाषा दीजिए।
उत्तर: पूंजीगत बजट वह बजट है जिसमें पूंजीगत मदों को शामिल किया जाता है।
प्र.48 वित्तीय बजट क्या है?
उत्तर: वित्तीय बजट सरकार की एक वर्ष की आय और व्यय का अनुमानित विवरण है।
प्र.49 माल तथा सेवाओं पर जीएसटी अप्रत्यक्ष कर क्यों है?
उत्तर: जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है और इसका भार उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित किया जा सकता है।
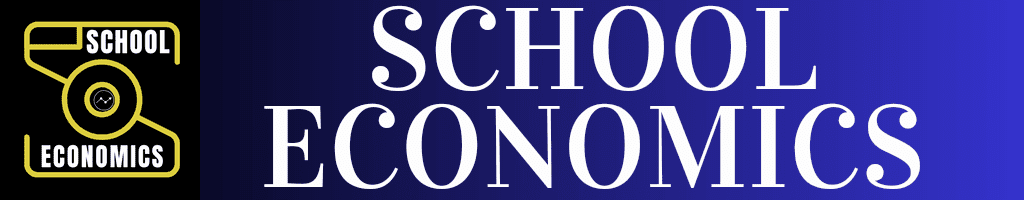


एक टिप्पणी भेजें